भारत में जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने का एक प्रमुख साधन भी है। बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित जातिगत जनगणना (Caste Census) का निर्णय न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह देश के सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और राजनीतिक रणनीतियों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
जातिगत जनगणना का तात्पर्य है जनसंख्या की जाति-आधारित गणना, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। भारत में 1931 के बाद से आधिकारिक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में जातिगत सर्वे जरूर करवाया था, लेकिन उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की गिनती होती रही है। पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य जातियों की संख्या का कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। जाति हमेशा से भारत की राजनीति का केंद्र रही है। विशेष रूप से उत्तर भारत में चुनावों में जातिगत समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जातिगत जनगणना से राजनीतिक दलों को स्पष्ट आंकड़े मिलेंगे, जिससे नीतिगत निर्णय अधिक तथ्यात्मक हो सकते हैं। यदि हम यह नहीं जानते कि OBC, SC, ST और अन्य वर्गों की वास्तविक संख्या क्या है तो आरक्षण और कल्याण योजनाओं का वितरण असमान हो सकता है। आंकड़ों के अभाव में नीतियां अनुमान के आधार पर बनती हैं। सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नौकरियों में आरक्षण और सामाजिक विकास योजनाओं को डेटा संचालित बनाना जातिगत जनगणना से संभव होगा।
बिहार सरकार ने 2023 में अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कराया था, जिसमें सामने आया कि राज्य में OBC और EBC की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 63% है। इसके बाद से कई राज्य सरकारों और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जनगणना कराने की मांग की। मोदी सरकार ने शुरू में इस मांग को टालते हुए “तकनीकी और संवैधानिक जटिलताओं” का हवाला दिया था, लेकिन 2025 में जब पश्चिम बंगला और बिहार चुनाव करीब हैं, तो यह निर्णय एक रणनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इससे भाजपा OBC मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है, जो लंबे समय से इस वर्ग की जनगणना की मांग कर रहे थे।
जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद यह मांग उठ सकती है कि OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। वर्तमान में OBC को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन यदि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक पाई जाती है, तो यह आंकड़ा पुनर्विचार की मांग कर सकता है। जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होने से समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। प्रत्येक जाति अपने अधिकार और प्रतिनिधित्व को लेकर सक्रिय हो सकती है, जिससे राजनीतिक दलों पर विशेष जातियों को लाभ पहुंचाने का दबाव बढ़ेगा। यदि आंकड़ों का दुरुपयोग हुआ, तो समाज में जातीय तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। उच्च और निम्न जातियों के बीच अधिकारों और संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जाति जनगणना केवल हिन्दुओं में होगी या मुस्लिम और इसाईयों की भी होगी।
जाति जनगणना की नकारात्मक बातों के साथ ही कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, जो आगे काफी लाभकारी होने वाली हैं। यदि सरकारों के पास सटीक आंकड़े होंगे, तो योजनाएं अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण होंगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। जातिगत आंकड़ों के आधार पर वंचित वर्गों की पहचान कर उन्हें लक्षित योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे समाज में जातिवाद और अधिक गहराएगा। जातिगत पहचान को प्राथमिक बनाना सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जाति का सत्यापन और डेटा संग्रहण एक बेहद कठिन और विवादास्पद कार्य हो सकता है। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है, जिससे वास्तविक सामाजिक उद्देश्यों से ध्यान भटक सकता है।
सवाल यह उठता है कि क्या जाति जनगणना संविधान के तहत हो रही है? विपक्ष लगातार संविधान और लोकतंत्र बचाने के दावे तो करता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि जाति गणना को लेकर संविधान क्या कहता है? वैसे तो संविधान में जातिगत जनगणना का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से इसे शामिल कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं (इंद्रा साहनी केस 1992) होने देने का निर्देश दिया है। ऐसे में यदि आंकड़ों के आधार पर आरक्षण में वृद्धि की मांग होती है, तो यह संवैधानिक बहस का विषय बन जाएगा। जातिगत जनगणना से जुड़े आंकड़े यदि पारदर्शी, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से एकत्र किए जाएं, तो यह सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसके लिए डेटा संग्रह की प्रक्रिया का निष्पक्ष होना जरूरी है। डेटा संग्रह के आंकड़ों का विश्लेषण स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किया जाए। साथ ही जाति आधारित लाभों को आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ जोड़ा जाए।
घोषणा के बाद अधिसंख्य जनसमूह का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा घोषित जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक और नीतिगत रूप से साहसी कदम है। यह निर्णय भारत के सामाजिक ढांचे, आरक्षण प्रणाली और राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकता है। हालांकि, इसके साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। जैसे सामाजिक एकता का बनाए रखना, आंकड़ों का दुरुपयोग रोकना और आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना। फिर भी यदि इसे सही नीयत और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए तो यह भारत के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और समतावादी बना सकता है।
रामगोपाल जाट
वरिष्ठ पत्रकार
#CasteCensusIndia #CasteBasedReservation #IndianReservationSystem #OBCReservation #SCSTOBCCensus #ModiGovernmentCasteCensus #CasteinIndianPolitics #ReservationPolicyIndia #MandalCommission #SocialJusticeinIndia #IndianCasteSystem #CastePolitics #SocioEconomicCasteCensus #BackwardClassesCensus #2025CasteCensus #BJPOBCStrategy #CasteandDemocracy #IndiaSocialStructure #InclusiveGovernanceIndia #CensusandPolicyMaking
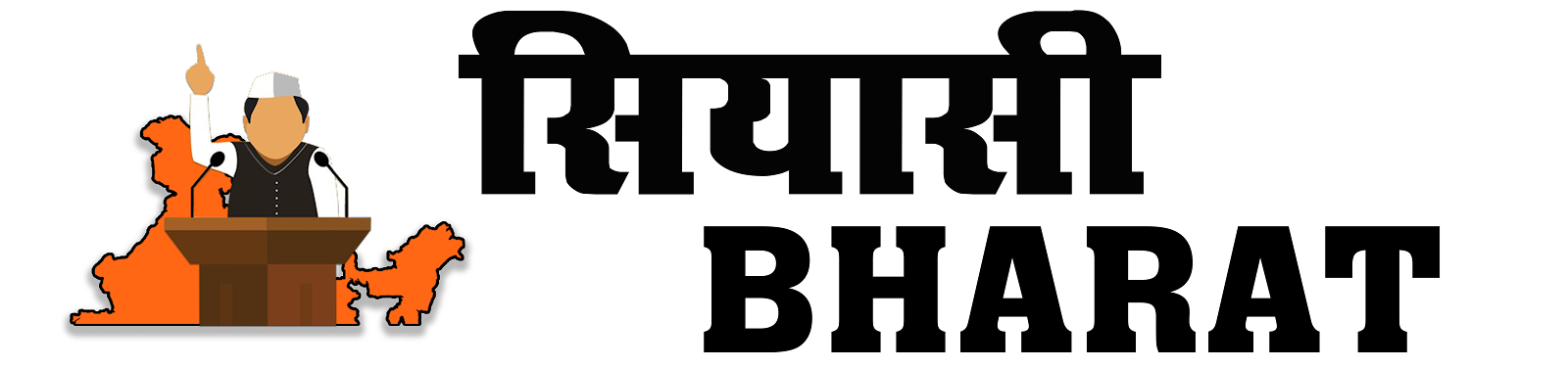

Post a Comment