तमिलनाडु में हाल ही में हुई कविन सेल्वगनेश की हत्या ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कविन, जो पल्लर समुदाय (अनुसूचित जाति) से आते थे, को मुक्कुलथोर समुदाय (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के सुरजित ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह यह थी कि कविन का सुरजित की बहन से प्रेम संबंध था। यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि भारत के उस कटु यथार्थ का हिस्सा है जहाँ जाति और पितृसत्ता की दीवारें आज भी प्रेम, रिश्तों और विवाह पर पहरा देती हैं।
इस घटना के बाद न केवल सामाजिक न्याय और महिला अधिकार समूहों ने आवाज़ उठाई है, बल्कि “ऑनर किलिंग” पर एक सख़्त और विशिष्ट क़ानून बनाने की माँग भी तेज़ हो गई है। यह माँग नई नहीं है, लेकिन हर ऐसी हत्या के बाद यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि आखिर भारत जैसे लोकतांत्रिक और आधुनिकता का दावा करने वाले समाज में प्रेम करना किसी की जान क्यों ले लेता है?
“इज़्ज़त” का सवाल: किसकी और कैसी इज़्ज़त?
ऑनर किलिंग शब्द अपने भीतर गहरी विडंबना समेटे हुए है। सवाल उठता है कि जब अनुसूचित जाति और आदिवासी महिलाओं पर 2017 से 2022 के बीच 27,000 से अधिक यौन हिंसा के मामले NCRB में दर्ज हुए, तो वहाँ “इज़्ज़त” की रक्षा करने वाले कहाँ थे?
दरअसल, यह तथाकथित इज़्ज़त स्त्रियों के शरीर और उनकी यौनिकता पर नियंत्रण से जुड़ी है। समाज में पुरुषों की सत्ता और जातिगत ऊँच-नीच की संरचना इसी नियंत्रण पर टिकी है। जब कोई महिला अपनी मर्ज़ी से, खासकर ऊँची जाति की महिला निचली जाति के पुरुष से रिश्ता बनाती है, तो यह पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। यही वह क्षण है जब “परिवार” और “समाज” हिंसा का सहारा लेकर “इज़्ज़त” बचाने का ढोंग रचते हैं।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य और दक्षिण एशिया की विशिष्टता
दुनिया भर में ऑनर आधारित हिंसा को जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। यह वह हिंसा है जहाँ महिला को सामाजिक और यौन नियमों को तोड़ने पर सज़ा दी जाती है। लेकिन भारत और दक्षिण एशिया में इसका चरित्र और भी जटिल है क्योंकि यहाँ जाति की गहरी जड़ें हैं।
यानी यहाँ इज़्ज़त केवल परिवार या समुदाय की नहीं, बल्कि जाति की होती है। जाति व्यवस्था की सत्ता विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के पास है। इनकी महिलाओं की “पवित्रता” ही उनकी जातिगत श्रेष्ठता की पहचान मानी जाती है। ऐसे में जब कोई दलित या पिछड़ी जाति का पुरुष इन महिलाओं से संबंध बनाता है, तो यह जातिगत प्रभुत्व के लिए सीधी चुनौती माना जाता है। यही कारण है कि भारत में ऑनर किलिंग की अधिकांश घटनाएँ ऐसे ही मेल-मिलाप को रोकने के नाम पर होती हैं।
आँकड़ों की हकीकत
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2020 से 2022 के बीच 76 ऑनर किलिंग की घटनाएँ दर्ज हुईं। परंतु वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है क्योंकि अधिकतर मामलों में हत्यारे पीड़िता के ही परिवार या रिश्तेदार होते हैं, और ये अपराध दबा दिए जाते हैं।
कुछ स्वतंत्र शोध बताते हैं कि हर साल दर्जनों से लेकर सैकड़ों हत्याएँ केवल इसलिए होती हैं कि किसी ने जाति, धर्म या गोत्र की दीवार तोड़कर प्रेम या विवाह किया। उत्तर भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में यह प्रवृत्ति ज्यादा स्पष्ट दिखती है, लेकिन दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं है।
आधुनिकता बनाम सामाजिक यथार्थ
भारत का संविधान हर नागरिक को प्रेम और विवाह की स्वतंत्रता देता है। विशेष विवाह अधिनियम (1954) जैसे कानून अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों को मान्यता देते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय आंदोलनों की लंबी परंपरा भी रही है।
इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि समाज में जाति और पितृसत्ता की जकड़न इतनी मज़बूत है कि कानून और आंदोलनों के बावजूद प्रेम और विवाह पर नियंत्रण कायम है। कविन की हत्या इस तथ्य को उजागर करती है कि तमिलनाडु जैसा प्रगतिशील राज्य भी इस हिंसा से अछूता नहीं है।
कानूनी प्रयास और उनकी सीमाएँ
ऑनर किलिंग पर विशेष कानून की माँग लंबे समय से होती रही है। कानून आयोग की 242वीं रिपोर्ट (2012) ने ‘प्रिवेंशन ऑफ़ इंटरफेरेंस विद फ्रीडम ऑफ़ मैट्रिमोनियल एलायंसेज़ (इन द नेम ऑफ़ ऑनर एंड ट्रेडिशन)’ नामक विधेयक का सुझाव दिया था।
सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ने 2022 में ‘फ्रीडम ऑफ़ मैरिज एंड एसोसिएशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ़ ऑनर क्राइम्स बिल’ का मसौदा तैयार किया।
इन विधेयकों में सामूहिक दबाव, धमकियों और हिंसा के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये सभी जाति स्तरों को समान रूप से अपराधी मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकतर मामले ऊँची जातियों द्वारा निचली जातियों के पुरुषों के खिलाफ होते हैं। यानी सबसे असुरक्षित वे जोड़े हैं जिनमें महिला अपेक्षाकृत ऊँची जाति से और पुरुष निचली जाति से आता है।
क्या केवल कानून काफी है?
कानून ज़रूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। ऑनर किलिंग को यदि केवल “सांस्कृतिक प्रथा” मानकर देखा जाएगा तो असली जड़ें छुप जाएँगी। इसे जाति और पितृसत्ता से पैदा हुई लैंगिक हिंसा के रूप में समझना होगा। जब तक समाज में जातिगत श्रेष्ठता और महिलाओं पर नियंत्रण की सोच बनी रहेगी, तब तक केवल कानून से समस्या हल नहीं होगी।
इसके लिए ज़रूरी है—
शिक्षा और संवेदनशीलता: स्कूल और कॉलेजों में जाति और लैंगिक समानता पर आधारित शिक्षा। पुलिस और न्यायपालिका का प्रशिक्षण: पुलिस को ऐसे मामलों को “परिवारिक मामला” कहकर नज़रअंदाज़ करने के बजाय गंभीर अपराध मानना होगा। राजनीतिक इच्छाशक्ति: दलित और महिला अधिकार आंदोलनों की माँगों को क़ानून और नीतियों में ईमानदारी से शामिल करना होगा। सुरक्षा तंत्र: अंतर-जातीय जोड़ों के लिए सुरक्षित आश्रय और त्वरित न्याय व्यवस्था।
निष्कर्ष: प्रेम की आज़ादी ही असली सामाजिक न्याय
कविन सेल्वगनेश की हत्या हमें यह याद दिलाती है कि भारत की आधुनिकता का चेहरा अधूरा है। जब तक कोई युवा अपनी मर्ज़ी से साथी चुनने के कारण मारा जाता है, तब तक यह दावा झूठा है कि हम जाति और पितृसत्ता से मुक्त हो गए हैं। ऑनर किलिंग के खिलाफ केवल कानून ही नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का बदलना भी ज़रूरी है। यह तभी संभव है जब हम जाति और पितृसत्ता की नींव को चुनौती दें और प्रेम की आज़ादी को वास्तविक अधिकार की तरह मान्यता दें। भारतीय लोकतंत्र का असली इम्तिहान यही है—क्या वह अपने नागरिकों को न सिर्फ़ वोट का अधिकार देगा, बल्कि प्रेम और जीवन की स्वतंत्रता भी सुरक्षित करेगा?
#HonorKilling #StopHonorKilling #EndHonorCrimes #JusticeForVictims #HumanRights #WomensRights #EqualityForAll #SayNoToViolence #EndPatriarchy #SaveDaughters #StopViolenceAgainstWomen #EndGenderBasedViolence #FreedomToChoose #RightToLove #JusticeMatters #NoMoreHonorKillings #EndOppression #StopKillingInTheNameOfHonor #LoveIsNotACrime #StopGenderViolence #ProtectHumanRights #EqualityNow #EndCruelty #BreakTheSilence #StopHateCrimes #StandForJustice #EndDiscrimination #HumanityFirst #ProtectWomen #RightToLive
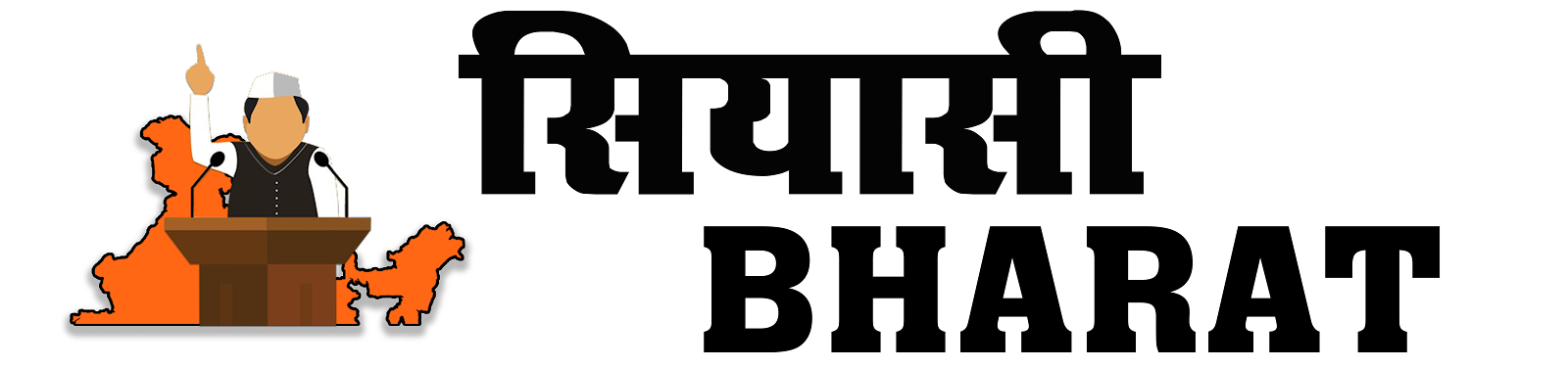

Post a Comment