हाल ही में अमेरिका ने भारत के उपर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां बार बार भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत के किसानों के हितों में लड़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता, वो मरते दम तक भारत के किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, और उनको पता है इसके कारण उनको बड़ी व्यक्तिगत क्षति होने वाली है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप भारत पर उंचा टैरिफ क्यों थोपना चाहते हैं, और किसानों के हितों में मोदी कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं।
वास्तव में देखा जाए तो भारत और अमेरिका की कृषि नीतियों की तुलना अपने-आप में एक दिलचस्प और जटिल विषय है। दोनों देश कृषि में भारी निवेश करते हैं, लेकिन दोनों की रणनीतियों, प्राथमिकताओं, संसाधनों और किसानों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में जमीन-आसमान का अंतर है। अमेरिका जहां 18.2 लाख पारिवारिक फार्मों को प्रतिवर्ष औसतन 27 लाख रुपये प्रति किसान सहायता देता है, वहीं भारत की सबसे बड़ी नकद सहायता योजना “पीएम-किसान” के तहत किसानों को केवल 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। यह अंतर न केवल आर्थिक है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किस तरह दोनों देश अपने किसानों को देखते हैं, उनकी समस्याओं को परिभाषित करते हैं, और उन्हें क्या महत्व देते हैं।
भारत में कुल 93.09 मिलियन, यानी लगभग 9.3 करोड़ कृषि परिवार हैं। ये परिवार न केवल कृषि में संलग्न हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में खेती एक संगठित और व्यावसायिक गतिविधि है, जिसमें उच्च तकनीक, सशक्त वित्तीय ढांचा और नीति आधारित समर्थन मौजूद है। अमेरिका में प्रति किसान आय करीब एक लाख डॉलर है, जबकि भारत में कोई केंद्रीकृत आय आँकड़ा मौजूद नहीं है। राज्यवार अध्ययन बताते हैं कि भारत के अधिकांश किसान परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से भी कम है। फिर भी WTO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बाजार खोलने और सब्सिडी घटाने का दबाव भारत पर ही ज्यादा बनाती हैं, जबकि अमेरिका को अपने भारी नकद हस्तांतरणों और अन्य लाभों के साथ नीति संचालन की खुली छूट मिली हुई है।
अमेरिका की नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह किसानों को सीधे नकद सहायता देता है, जिसमें कोई खरीद नहीं होती। उदाहरण के लिए, PLC, यानी Price Loss Coverage, ARC, यानी Agriculture Risk Coverage, DMC, यानी Dairy Margin Coverage, फसल बीमा, व्यापार राहत और आपदा सहायता कार्यक्रम सीधे किसानों के खातों में पैसे भेजते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाना और बाजार के उतार-चढ़ाव से उनकी रक्षा करना है। इसके अलावा जब कोई आपदा या व्यापारिक संकट आता है, तब अमेरिका विशेष राहत पैकेज के रूप में भी अरबों डॉलर की सहायता किसानों को देता है। 2020 में कोविड महामारी के दौरान अमेरिका ने अपने किसानों को 45.6 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड मदद दी थी। भारत में उस दौरान विशेष राहत नहीं दी गई, सिवाय कुछ राज्यों द्वारा अस्थायी राहत घोषणाओं के।
भारत की कृषि सब्सिडी का ढांचा पूरी तरह अलग है। यहां सरकार मुख्य रूप से इनपुट सब्सिडी देती है, जैसे कि उर्वरक, पानी, बिजली, बीज, सिंचाई योजनाएं, आदि। इसके अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किए जाते हैं, जो कुछ फसलों पर सरकारी खरीद के माध्यम से किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देते हैं। साथ ही, पीएम-किसान योजना के तहत हर पात्र किसान को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में दिए जाते हैं। वर्ष 2023–24 में भारत सरकार ने कुल कृषि सहायता के रूप में 5 लाख करोड़ रुपये, यानी 57.5 बिलियन डॉलर का बजट निर्धारित किया था, जो अमेरिका के 42.4 बिलियन डॉलर अनुमानित खर्च से अधिक है, लेकिन चूंकि भारत में किसानों की संख्या अमेरिका से 50 गुना अधिक है, इसलिए प्रति किसान औसत लाभ बहुत ही कम हो जाता है।
इस असमानता का दूसरा पक्ष यह है कि भारत में कृषि को “जीविका” के रूप में देखा जाता है, जबकि अमेरिका में यह एक “व्यवसाय” है। भारतीय किसान अक्सर छोटे जोत वाले, कर्ज में डूबे, मानसून पर निर्भर और बाजार की अनिश्चितताओं से पीड़ित होते हैं। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए न तो पर्याप्त बीमा सुरक्षा उपलब्ध है, न ही जोखिम साझा करने की सक्षम नीति। भारत का फसल बीमा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी तक प्रभावी रूप से किसानों को राहत नहीं दे पाया है। निजी बीमा कंपनियों के लाभ के आरोप भी इस योजना को सवालों के घेरे में लाते हैं। वहीं अमेरिका में कृषि बीमा में 53.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, जिससे हर छोटे-बड़े किसान को उनकी उपज का बाजार भाव गिरने पर आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
भारत में खेती एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। किसान आत्मनिर्भरता, परिश्रम और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक हैं, लेकिन यह सम्मान नीतियों में नहीं झलकता। दूसरी ओर अमेरिका में किसान नीति का एक केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक क्षमता और राजनीतिक लॉबिंग बहुत प्रभावशाली है। अमेरिकी कृषि लॉबी वाशिंगटन में नीतियों को प्रभावित करने की भरपूर ताकत रखती है। इसी का परिणाम है कि WTO जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका खुलेआम सब्सिडी देकर भी यह तर्क देता है कि विकासशील देशों को बाजार खोलने चाहिए। वह भारत पर यह दबाव डालता है कि वह अपनी MSP व्यवस्था को बंद करे, अपनी कृषि सब्सिडियों को WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार सीमित करे और किसानों को दी जा रही सहायता को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में “बाधा” के रूप में देखा जाए।
भारत WTO में “विशेष और भिन्न उपचार” (Special & Differential Treatment) का लाभ पाता है, जो विकासशील देशों को कुछ रियायतें देता है। परंतु यह रियायतें बहुत सीमित हैं और बार-बार अमेरिका और यूरोपीय संघ इन छूटों को चुनौती देते रहे हैं। भारत को अक्सर अपनी खाद्य सुरक्षा योजनाओं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), और MSP, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद नीति को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है। जबकि अमेरिका, जो खुले तौर पर हर साल अरबों डॉलर अपने किसानों को सीधे देता है, WTO में खुद को ‘कानूनी’ सहायता देने वाला बताता है।
वास्तव में यह पूरी बहस न केवल सब्सिडी की राशि की है, बल्कि नीति दर्शन की भी है। भारत की नीति अभी भी एक औपनिवेशिक सोच के ढांचे से निकल नहीं पाई है, जिसमें खेती को ‘गरीब की मजबूरी’ माना जाता है, न कि ‘आर्थिक उत्पादन की ताकत’। नीति निर्धारण में उद्योगों और कॉरपोरेट्स को मिलने वाली सब्सिडी को ’निवेश’ कहा जाता है, जबकि किसान को मिलने वाली मदद को ‘बोझ’ माना जाता है। यह मानसिकता तब और अधिक खतरनाक हो जाती है, जब कृषि संकट के शिकार किसान आत्महत्या करते हैं और सरकारें उन्हें महज आंकड़ों की तरह प्रजंटेशन करती हैं।
अमेरिका और भारत की तुलना इसलिए जरूरी है, क्योंकि दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जहां कृषि का सामाजिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है, पर यह तुलना हमें यह भी बताती है कि अगर हम केवल बजट के आंकड़े देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि भारत में कृषि पर खर्च अमेरिका से ज्यादा है, तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि यह खर्च किस पर, कैसे और कितना प्रभावी रूप से किया जा रहा है। अमेरिका अपने छोटे किसान वर्ग को भी एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए सशक्त नीति, नकद सहायता और बीमा कवच देता है। भारत में किसान अभी भी बिचौलियों, कर्ज, मौसम की मार और बाजार के उतार-चढ़ाव से खुद को बचा नहीं पाता।
भारत में यदि कृषि को वास्तव में मजबूत बनाना है, तो उसे केवल इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम मूल्य की गारंटी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता, लचीली बीमा योजनाएं, जोखिम में साझेदारी, कृषि अनुसंधान और टेक्नोलॉजी का लाभ, और बाजार तक सीधी पहुंच जैसे बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा ढांचा भी चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सम्मान में सुधार लाए। इस व्यापक परिवर्तन के बिना भारत कृषि संकट से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम WTO में केवल संरक्षण की गुहार लगाते रहेंगे और अपने किसानों को पर्याप्त आर्थिक सम्मान नहीं देंगे, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी स्थिति लगातार कमजोर होती जाएगी। अमेरिका जैसे देश अपने सब्सिडी आधारित मॉडल के बावजूद ‘फ्री ट्रेड’ के पैरोकार बने रहेंगे। असल में देखा जाए तो अमेरिका का भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में “निवेश” करने की मंशा अपने आर्थिक हितों से प्रेरित है, न कि भारत के किसानों की बेहतरी से। अमेरिका यहां पूंजी निवेश नहीं करना चाहता, बल्कि अपने कृषि और डेयरी उत्पादों का एक विशाल बाजार चाहता है। इसके पीछे उसकी रणनीति साफ है। अपने किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का बोझ कम करना और विदेशी बाज़ारों के ज़रिए उन्हें अधिक लाभ दिलाना।
वर्तमान में अमेरिका अपने प्रत्येक किसान को औसतन 27 लाख रुपये सालाना की प्रत्यक्ष सहायता देता है, जबकि भारत के किसान को केवल 6,000 रुपये सालाना पीएम-किसान योजना के तहत मिलते हैं, और वह भी सभी किसानों को नहीं। इसके अलावा भारत में उर्वरक, बिजली और सिंचाई जैसी इनपुट सब्सिडी दी जाती है, जो किसान के लिए कुछ राहत जरूर है, लेकिन उनकी आमदनी को टिकाऊ और सम्मानजनक नहीं बनाती। अगर अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में खुला बाज़ार मिल गया, तो इससे भारत के स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की उच्च तकनीक, सब्सिडी-समर्थित उत्पादन और कम लागत के चलते वह भारतीय उत्पादों से सस्ती दर पर बाज़ार पर कब्ज़ा कर सकता है। इससे न केवल भारत का आत्मनिर्भर कृषि और डेयरी ढांचा कमजोर होगा, बल्कि करोड़ों किसानों और पशुपालकों की आजीविका पर भी संकट आ सकता है। भारत सरकार को इस “निवेश” के पीछे की असल मंशा को समझते हुए, अपने किसानों की रक्षा करनी चाहिए। बाज़ार खोलने से पहले यह ज़रूरी है कि भारतीय किसान आर्थिक रूप से सक्षम, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनें, नहीं तो यह साझेदारी नहीं, वर्चस्व बनकर रह जाएगी।
इसलिए भारत अब केवल रक्षा की मुद्रा में न रहे, बल्कि कृषि में साहसिक सुधार करे, ऐसा सुधार जो किसान को उपभोक्ता या वोट बैंक नहीं, बल्कि एक सम्मानित नागरिक और आर्थिक निर्माता के रूप में देखे। तभी भारत की कृषि नीतियाँ वैश्विक मंच पर प्रभावी चुनौती बन सकेंगी, न कि केवल प्रतिक्रिया। ऐसे में भारत को अपने संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों को पुनः परिभाषित करना होगा, ताकि अगली बार जब अमेरिका सब्सिडी की बात करे, तो भारत मजबूरी में नहीं, आत्मविश्वास से जवाब दे सके।
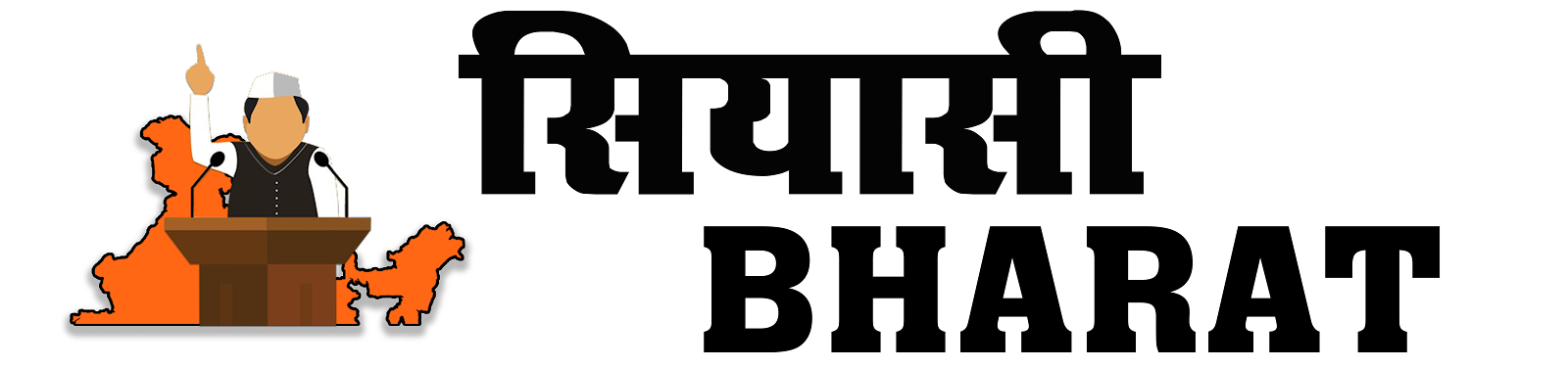

Post a Comment